साधु शब्द ऋग्वेद और अथर्ववेद में प्रकट होता है, जहां इसका अर्थ है सीधा, सही, सीधे लक्ष्य तक ले जाना । वैदिक साहित्य की ब्राह्मण परत में, यह शब्द किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो अच्छी तरह से व्यवस्थित, दयालु, इच्छुक, प्रभावी या कुशल, शांतिपूर्ण, सुरक्षित, अच्छा, गुणी, सम्माननीय, धर्मी, महान है। हिंदू महाकाव्यों में, इस शब्द का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो संत, ऋषि, द्रष्टा, पवित्र व्यक्ति, गुणी, पवित्र, ईमानदार या सही है।
साधू शब्द का मूल शब्द साध है जो संस्कृत से लिया गया है। साध शब्द का अर्थ है "सीधे बनो" या "किसी लक्ष्य तक पहुंचो"। परंतु हिन्दू धर्म में साधु शब्द का अर्थ है एक भिक्षुक, तपस्वी या किसी भी पवित्र व्यक्ति से है जिसने भगवान को पाने के लिए संसार का मोह त्याग त्याग दिया हो।
चूँकि किसी भी ऊँचे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अनुशासित और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, एक साधु को शाब्दिक रूप से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसने अपना पूरा जीवन एक साधना, या आध्यात्मिक अनुशासन के मार्ग के लिए समर्पित कर दिया है। हालांकि इन विषयों के रीति-रिवाज और प्रथाएं संप्रदाय या परंपरा के अनुसार भिन्न हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप आदत और पोशाक की एक विस्तृत श्रृंखला होती है, प्रत्येक सच्चे साधु का लक्ष्य - आध्यात्मिकता के मार्ग पर दृढ़ता से स्थिर रहना - अंततः एक ही है।
जीवन का अंतिम उद्देश्य, हिंदू ग्रंथों के अनुसार, सांसारिक आसक्तियों को छोड़ना, भौतिक अहंकार को पार करना और परमात्मा (हमारे आध्यात्मिक स्रोत) के साथ फिर से जुड़ना है - दूसरे शब्दों में, साधु का मार्ग अपनाना।
लेकिन क्योंकि इस तरह के मोहों को छोड़ना बहुत कठिन है, वेद जीवन को चार आश्रमों, या प्रगतिशील चरणों में विभाजित करते हैं, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति धीरे-धीरे अपनी स्वार्थी इच्छाओं को छोड़ना सीख सकता है ताकि वे अंततः मुक्ति प्राप्त कर सकें।
पहला चरण, जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है, आम तौर पर पाँच साल की उम्र में शुरू होता है, जब एक बच्चे को एक गुरुकुल (प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली) में भेजा जाता था, जहाँ वे एक शिक्षक / गुरु के साथ रहते और उनकी सेवा करते थे, जो बदले में उस बच्चे को सांसारिक, और उससे भी महत्वपूर्ण, आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते थे। एक दयालु और प्यार करने वाले शिक्षक की ईमानदारी से सेवा करने की प्रक्रिया के माध्यम से, छात्र अनुशासन का मूल्य सीखते थे, और उन्हें
यह भी सिखाया जाता था की निस्वार्थता की आदतों का निर्माण कैसे करें एवं भविष्य के आध्यात्मिक विकास की नींव कैसे रखें।
अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, युवा वयस्क दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, जिसे गृहस्थ आश्रम (विवाहित जीवन) के रूप में जाना जाता है। अपने सांसारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक स्वस्थ आउटलेट प्रदान करने के अलावा, एक साथी और बच्चे होने के कर्तव्य एक व्यक्ति को दूसरों की जरूरतों पर ध्यान देने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। जैसे-जैसे हमारी जिम्मेदारियों का दायरा सिर्फ गुरु से एक परिवार तक विस्तृत होता जाता है, वैसे-वैसे दूसरों की भलाई के बारे में विचार करने की हमारी क्षमता भी बढ़ती जाती है, जिससे हम और भी अधिक आध्यात्मिक विकास कर पाते हैं।
एक बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियां स्वाभाविक रूप से समाप्त होने लगती हैं, तो शास्त्र हमें वानप्रस्थ नामक जीवन के तीसरे चरण में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वाना का अर्थ है "जंगल," और प्रस्थ का अर्थ है "जाना", वानप्रस्थ आश्रम तब होता है जब कोई व्यक्ति शहर से बाहर एकांत स्थान पर जाकर सांसारिक जुड़ाव से खुद को अलग करना शुरू कर देता है जहाँ योग और ध्यान का अभ्यास न्यूनतम विकर्षण के साथ किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि परिवार में हर कोई भावनात्मक और आर्थिक रूप से सुरक्षित है, वानप्रस्थ में एक व्यक्ति संन्यास लेने की तैयारी की प्रक्रिया शुरू करता है, या जीवन के चौथे चरण में प्रवेश करता है जिसमें एक व्यक्ति पारिवारिक जीवन से पूरी तरह से सेवानिवृत्त हो जाता है, एक त्यागी बन जाता है, और पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है एक साधु का जीवन।
जबकि पहले तीन चरण एक को अंततः एक त्यागी बनने की दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं, वे किसी भी तरह से एक आवश्यकता नहीं हैं। किसी भी उम्र, या आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि का व्यक्ति साधु बन सकता है, बशर्ते कि उनमें सच्ची इच्छा हो, और वह वास्तव में मार्ग का अनुसरण करने में सक्षम हो।
गुरु - "अंधेरे को दूर करने वाले" के रूप में अनुवादित, गुरु शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो आध्यात्मिक ज्ञान की मशाल से आपके अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकता है। परंपरागत रूप से, केवल एक व्यक्ति जो स्वयं उच्च स्तर की आध्यात्मिक जागृति से गुजर चुका था, ऐसी मशाल पकड़ सकता था।
ऋषि - एक ऋषि वह होता है, जो ध्यान की गहन अवधि के माध्यम से उच्च स्तर की दिव्य अनुभूति प्राप्त करने के बाद, भजनों और कविताओं की रचना करके इस तरह की अनुभूति को साझा करने और व्यक्त करने के लिए प्रेरित हो जाता है। एक ऋषि, दूसरे शब्दों में, एक ऐसा व्यक्ति है जो एक आध्यात्मिक वाहन के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से दिव्य ज्ञान प्रवाहित हो सकता है और दूसरों तक पहुँचाया जा सकता है।
स्वामी - "गुरु" के रूप में अनुवादित, स्वामी एक ऐसी उपाधि है जिसे इंद्रियों का स्वामी माना जाता है, और इस प्रकार सांसारिक इच्छाओं से अप्रभावित आध्यात्मिकता के मार्ग का अनुसरण करने में सक्षम है।
पंडित - जिसका अर्थ है "बुद्धिमान," "सीखा," या "शिक्षित," शब्द पंडित का उपयोग आध्यात्मिकता के किसी विशेष विषय में विशेष ज्ञान रखने वाले को सम्मानित करने के लिए किया जाता है।
आचार्य - एक विशेष रूप से शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, एक आचार्य वह होता है जो उदाहरण के लिए शिक्षण और नेतृत्व के लिए जाना जाता है।
दु:ख की बात है कि संसार में ऐसे लोग भी हैं जो एक विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करके और चतुराई से बोलकर साधकों को उनकी सेवा और पूजा करने के लिए बहकाते हैं। इसलिए, यह सीखना महत्वपूर्ण है कि सच्चे साधुओं को उनके सम्मानजनक उपाधियों के आधार पर नहीं, बल्कि उनके गुणों, जैसे सहिष्णुता, करुणा और सभी के प्रति मित्रता के आधार पर पहचाना जाए। शांत, और शास्त्रों का पालन करते हुए, एक साधु पूरी तरह से भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, और इस प्रकार दूसरों की दया और दान पर निर्भर करता है, बदले में जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार: आध्यात्मिक ज्ञान देता है।
हिंदू धर्म के भीतर कई हजार परंपराओं से जुड़े लाखों साधु हैं। अधिकांश, हालांकि, मोटे तौर पर वैष्णव (विष्णु की पूजा करने वाले), या शैव (जो शिव की पूजा करते हैं) के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं।
जबकि इन दो समूहों के भीतर और बाहर कई और विभाजन मौजूद हैं, आश्रम या मंदिर में रहने, ड्रेडलॉक या उलझे हुए बाल रखने और नारंगी रंग के रंगों को पहनने जैसी असंख्य प्रथाएं कई लोगों के लिए आम हैं।
ऐसा कहने के बाद, कुछ रीति-रिवाज विशेष समूहों के लिए अधिक सामान्य हैं। हालांकि यह सच है कि वैष्णव परंपरा के भीतर ऐसे लोग हैं जो उलझे हुए बाल रखते हैं, कई ऐसे भी हैं जो मुंडा सिर भी रखते हैं - शैव परंपराओं के भीतर आमतौर पर इसका पालन नहीं किया जाता है। वैष्णव साधु भी आम तौर पर बहुत साफ रहना पसंद करते हैं, जबकि शैव परंपराओं में कई, जैसे नागा बाबा और अघोरी, अपने शरीर को राख से ढँक देते हैं। नागा नग्न रहने और खुद को ठंडे तापमान के अधीन करने के लिए भी जाने जाते हैं, जबकि अघोरी मानव खोपड़ी का उपयोग कटोरे के रूप में करने के लिए कुख्यात हो गए हैं।
यद्यपि सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है और इस प्रकार प्रकृति में आध्यात्मिक है, जीवन के द्वैत - जैसे गर्म / ठंडा, बूढ़ा / युवा, बदसूरत / सुंदर, आदि - कई लोगों में आकर्षण और घृणा की चेतना पैदा करते हैं जो पूरी तरह से भौतिक पदनामों पर आधारित है। इन शैव समूहों द्वारा प्रतीत होने वाले अपरंपरागत/अत्यधिक रीति-रिवाज इसलिए अभ्यासियों को आकर्षण/घृणा की सांसारिक धारणाओं को पार करने में मदद करते हैं जो अक्सर किसी को और सब कुछ जोड़ने वाली दिव्य वास्तविकता को समझने से विचलित करते हैं।
अंतत:, जिस भी संप्रदाय का साधु विशेष रूप से एक हिस्सा है, हर वास्तविक अभ्यास का मूल बिंदु अनिवार्य रूप से एक ही है - सांसारिक जीवन की अस्थिरता को याद दिलाने के लिए, ताकि कोई बेहतर तरीके से परमात्मा के साथ जुड़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर सके।
साधु बनना शुरू होता है, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने की सच्ची इच्छा के साथ। यदि किसी व्यक्ति में ऐसी इच्छा प्रबल रूप से प्रकट होती है, तो उस व्यक्ति को एक सच्चे गुरु की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो सफलता के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान कर सके।
किसी प्रकार की सेवा या सेवा करने का प्रयास करके विनम्रतापूर्वक गुरु के पास जाना चाहिए, जिसे अगर ईमानदारी से निष्पादित किया जाए, तो गुरु की प्राकृतिक करुणा और आध्यात्मिक मामलों पर निर्देश देने की इच्छा पैदा हो सकती है। ऐसी सेवा एक व्यक्ति को उक्त निर्देशों को प्राप्त करने और आत्मसात करने के लिए आवश्यक विनम्रता को बेहतर ढंग से विकसित करने में भी मदद करती है।
प्रतिबद्ध, ईमानदार और विनम्र बने रहने वाला सच्चा साधु, जो हमेशा समाज के आध्यात्मिक कल्याण के लिए चिंतित और जिम्मेदार महसूस करता है, उसे मार्गदर्शन देने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित किया जाएगा। इस तरह के मार्गदर्शन के माध्यम से ही लोग अंततः स्वयं साधु बन सकते हैं। जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है, "जब छात्र तैयार होगा, शिक्षक प्रकट होगा।"
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। Dharmsaar इसकी पुष्टि नहीं करता है।)
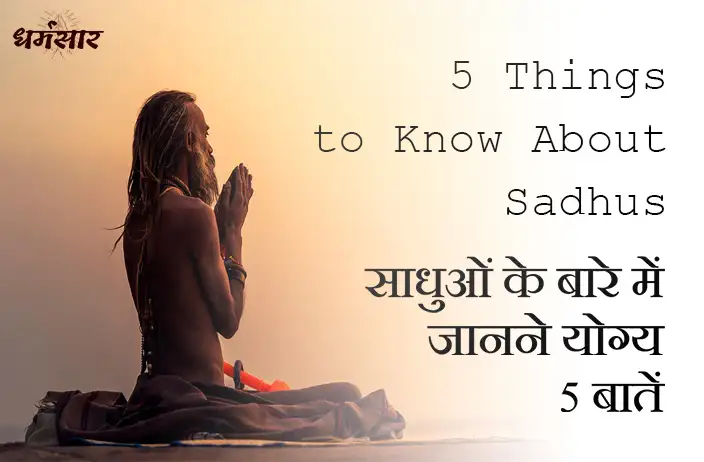
 डाउनलोड ऐप
डाउनलोड ऐप